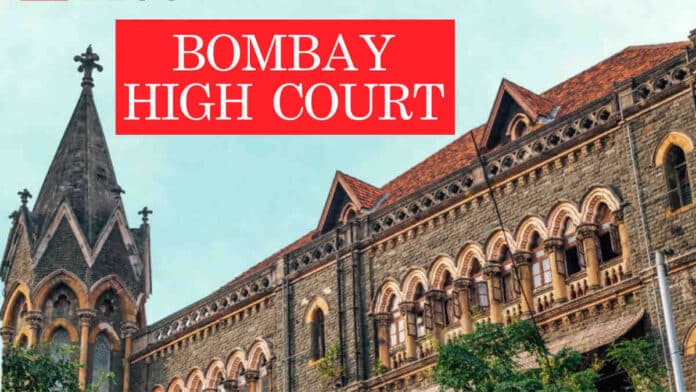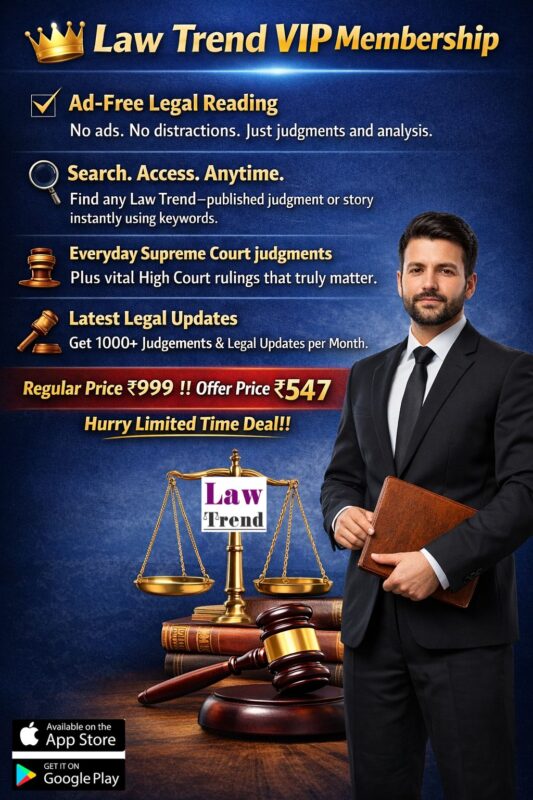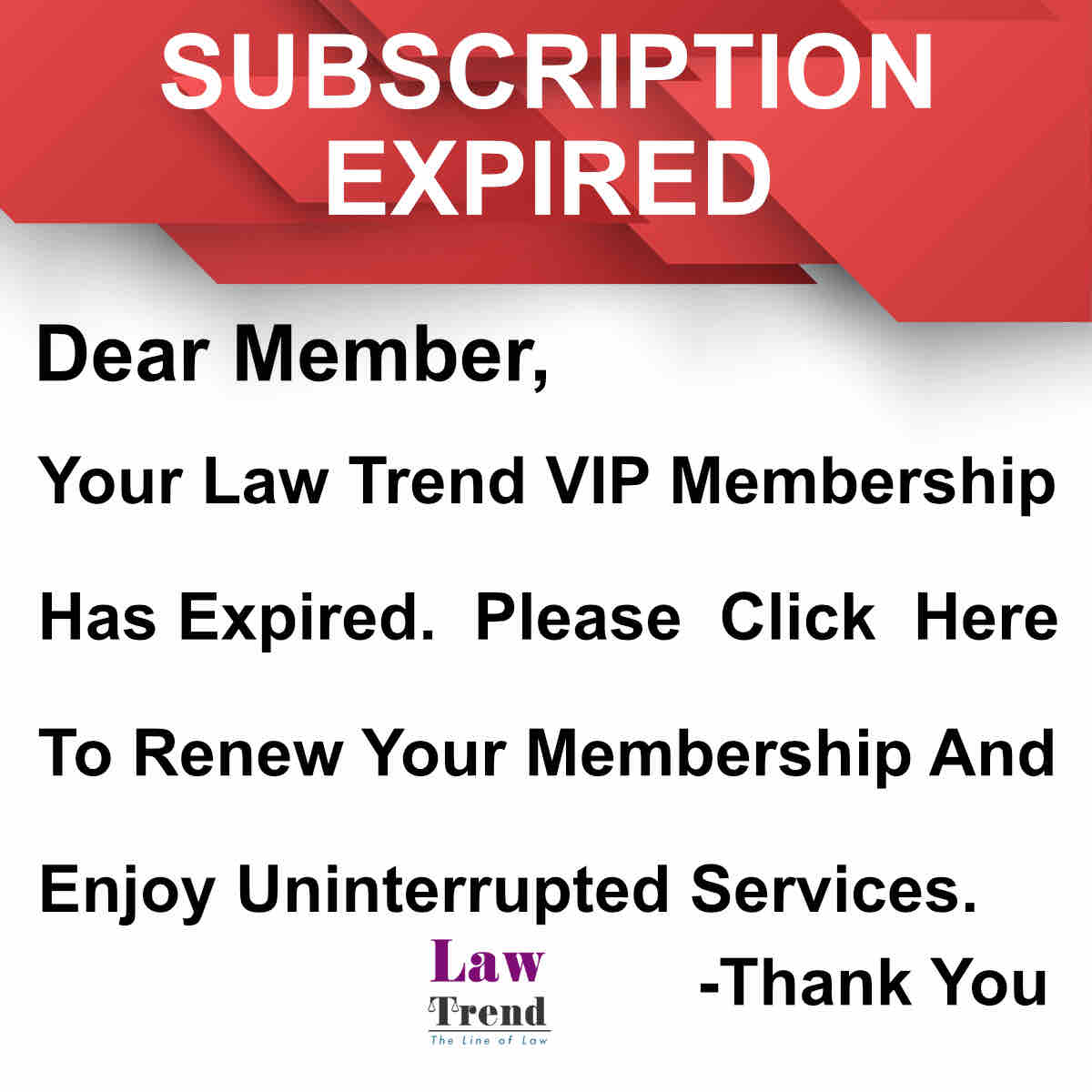बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का दायरा उस राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता है जहां किसी व्यक्ति को समुदाय का हिस्सा घोषित किया जाता है, और कहा कि अन्यथा धारण करने से इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। अधिनियमन.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था और इसका उद्देश्य एक वर्ग के सदस्यों को मिलने वाले अपमान और उत्पीड़न को दूर करना और सुनिश्चित करना था। उन्हें मौलिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकार।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) का दायरा उस राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता जहां किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य घोषित किया गया हो।
अदालत ने कहा, “देश के किसी अन्य हिस्से में, जहां अपराध हुआ है, व्यक्ति अधिनियम के तहत सुरक्षा का भी हकदार है, हालांकि उसे वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।”
पूर्ण पीठ ने यह भी माना कि सजा की परवाह किए बिना अधिनियम के तहत दायर सभी अपीलें उच्च न्यायालय की एकल पीठ के अधिकार क्षेत्र में होंगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जाति स्वचालित रूप से किसी व्यक्ति से चिपक जाती है क्योंकि वह उस जाति या समूह से संबंधित दो व्यक्तियों से पैदा हुआ है।
“किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति के लिए अपनी जाति के बोझ से छुटकारा पाना संभव नहीं है, भले ही वह व्यावसायिक समूह से बाहर आ जाए या उस विशेष जाति की सामाजिक स्थिति से बाहर आ जाए और सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए अपनी जाति में अपने साथियों से आगे निकल गया,” पीठ ने कहा।
“अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जन्मे व्यक्ति पर लगा लेबल उसके व्यक्तिगत उत्थान, उसके अपने अच्छे कर्मों से उसके सामाजिक उत्थान के बावजूद जारी रह सकता है, लेकिन वह अपनी पहचान और अस्मिता को नहीं खोता है, जैसा कि एक समय उसे भुगतना पड़ा था।” दंश और नुकसान के बावजूद, उन्होंने जीवन में आगे की यात्रा की है,” यह जोड़ा गया।
अत्याचार अधिनियम तब अधिनियमित किया गया, जब यह महसूस किया गया कि जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य संविधान के तहत उन्हें उपलब्ध कराए गए अधिकारों का दावा करते हैं और वैधानिक सुरक्षा की मांग करते हैं, तो उन्हें डराया जाता है, डराया जाता है और उनका मोहभंग किया जाता है और यहां तक कि आतंकित किया जाता है। अपमान सहना होगा, अदालत ने कहा।
इसमें कहा गया है कि इन जातियों के लोगों को क्रूर घटनाओं का शिकार बनाया गया है, उन्हें उनके अधिकार और संपत्ति से वंचित किया गया है और उन्हें अपमान, अपमान और उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है।
“जातिविहीन समाज का निर्माण, जहां एक व्यक्ति समान व्यवहार का हकदार हो, स्वतंत्र भारत के लिए हासिल किया जाने वाला अंतिम सपना है, ताकि मानव का एक वर्ग मौजूद रहे और देश के सभी नागरिकों को मुक्ति मिले और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने कहा था का सपना देखा,” यह कहा।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि यदि व्यक्ति (पीड़ित) अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है तो अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध लागू नहीं होगा।
हालाँकि, महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने इस तर्क का विरोध किया कि जाति का बोझ एक व्यक्ति द्वारा बरकरार रखा जाता है और चूंकि क़ानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किए गए अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए अधिनियम के तहत अपराध आकर्षित होगा। प्रवासन की परवाह किए बिना.
पीठ ने याचिकाकर्ताओं के मामले को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, ‘यह तर्क कि जाति एक राज्य की सीमाओं तक ही सीमित होगी, एक मिथक होगा।’
फैसले में कहा गया, “अत्याचार अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की मानवीय गरिमा की रक्षा करने का हकदार है और किसी भी मामले में, उनकी स्थिति को केवल एक विशेष राज्य तक सीमित रखते हुए, प्रतिबंधित या संकुचित अर्थ का हकदार नहीं है।”
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वह एक संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण निर्माण को अपनाता है तो यह एक गंभीर दोष होगा, जो कानून के इरादे को धूमिल कर देगा और इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की पहचान को मूल राज्य तक सीमित करना संविधान के मौलिक अधिकारों को पराजित करेगा, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपने मूल राज्य से ही बांध दिया जाएगा और बाहर जाकर खुद को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
Also Read
अदालत ने कहा, “यह निश्चित रूप से पहचाने गए वर्ग को उच्च वर्ग के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और समानता प्राप्त करने में सहायता करने की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि संविधान में निहित है।”
पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था एक “अजीब और जटिल चीज़” है।
इसमें कहा गया है कि परंपरा से बंधी जाति व्यवस्था के भ्रूण में अस्पृश्यता की संस्था जटिल रूप से मौजूद थी, जिसने हिंदुओं को विभाजित किया, उनकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित किया और संपर्क करके अपवित्र करने की पारंपरिक मान्यता को दृढ़ता से बढ़ावा देकर मानवता के दमन और दासता को उनके दिमाग में गहराई से अंकित किया। वह व्यक्ति, जो उच्च जाति के किसी सदस्य के साथ भोजन करता है या पानी पीता है और इस प्रकार, अछूत वर्ग को अपमानित करते हुए, छोटे-मोटे काम करता है।
पीठ ने कहा कि इतिहास दर्शाता है कि ऊंची जाति के लोग छुआछूत का पालन करके समाज के निचले तबके को दूर रखते थे और सामाजिक ढांचे में उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे।
अदालत ने कहा, “अस्पृश्यता की प्रथा चाहे किसी भी रूप में हो, यह संबंधित लोगों के लिए अपमानजनक अपील के समान है।”
अधिनियम का उद्देश्य एक वर्ग के खिलाफ किए गए अपराधों की जाँच करना और उन्हें रोकना था और यह कोई ऐसा कानून नहीं है जो कोई लाभ या विशेषाधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें विभिन्न आक्रामक कृत्यों, अपमान, अपमान और उत्पीड़न के अधीन होने से रोकने के लिए एक अधिनियम है। विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का लेखा-जोखा।