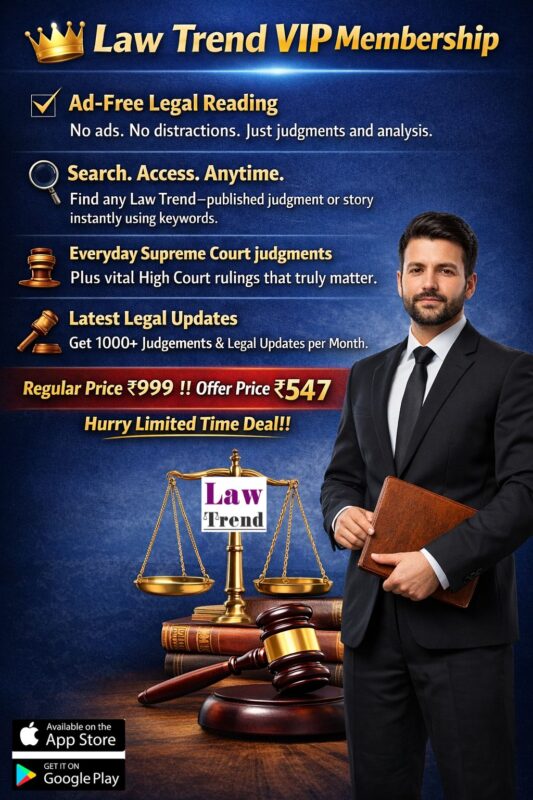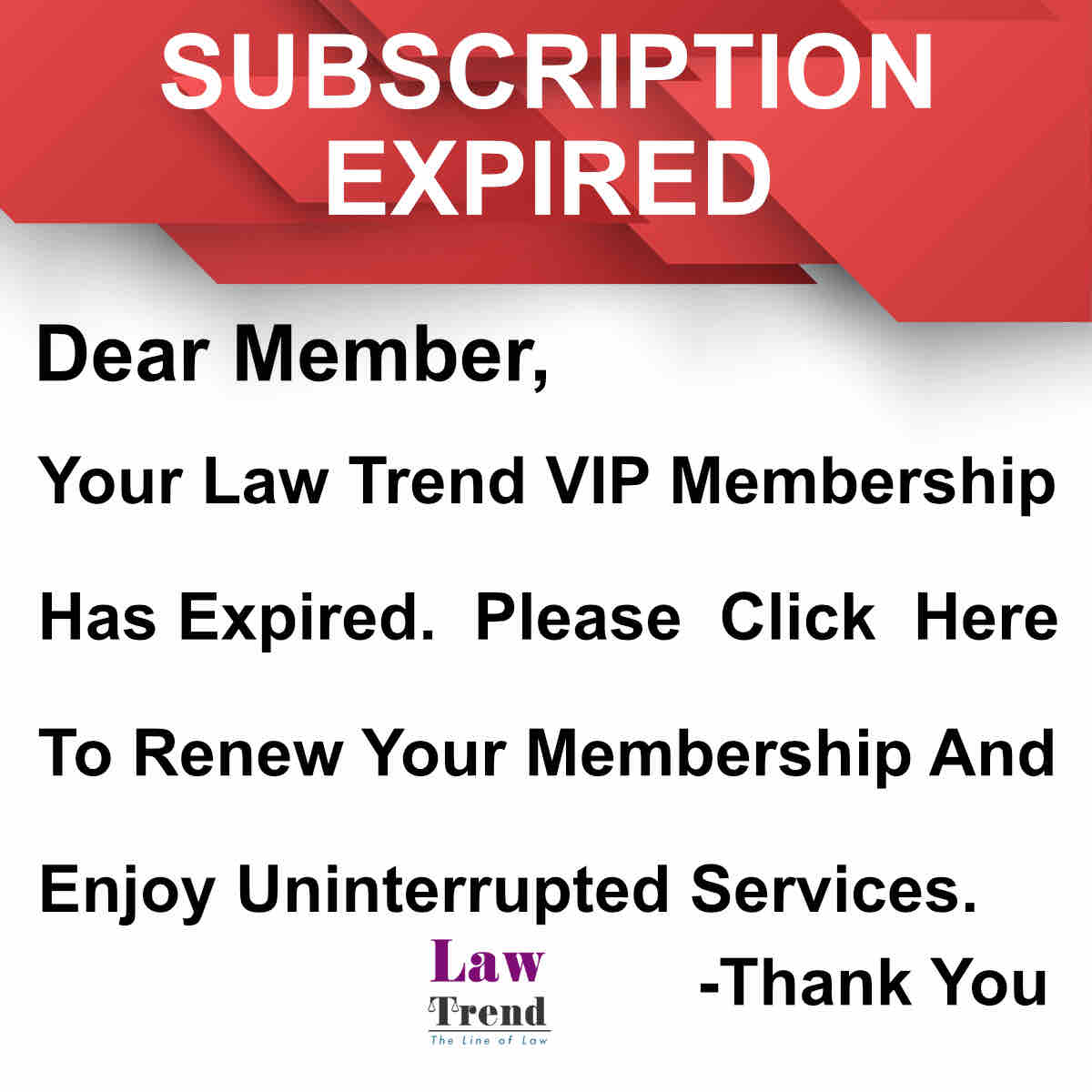भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है न्यायपालिका संविधान का एक हिस्सा है। न्यायपालिका नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। यह अंतिम प्राधिकरण है जहां संवैधानिक आदेश के तहत नागरिकों को कानूनी मामलों में न्याय मिल सकता है।
यह नागरिकों, राज्यों और अन्य पक्षों के बीच विवादों पर कानून लागू करने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट हो या जिला स्तरीय कोर्ट, ये देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं।
इस न्यायिक प्रणाली में जिला स्तर पर न्याय दिलाने का कार्य जजों और मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता है। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। हालाँकि, एक जज और मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कार्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय II, आपराधिक न्यायालयों और अधिकारी के संविधान से संबंधित है।
यहां हम आपको दोनों के कार्यों और अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
आपराधिक न्यायालयों के वर्ग:
धारा 6 सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी कानून के तहत गठित उच्च न्यायालयों और न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में, आपराधिक न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:
- सत्र न्यायालय;
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और, किसी भी महानगरीय क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट;
- द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; और
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जज और मजिस्ट्रेट चयन प्रक्रिया– आम तौर पर
संविधान के अनुसार, भारतीय न्यायिक प्रणाली में तीन परत वाली अदालत प्रणाली होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जिला जज बनने के लिए आपके पास कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कानून की प्रैक्टिस करने का सात साल का अनुभव होना चाहिए। जिसके बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं।
न्यायिक सेवा परीक्षा, जिला या अधीनस्थ न्यायालय परीक्षा भारत के हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।
वहीं, कोई भी छात्र कानून की डिग्री लेने के बाद सीधे पीसीएस-जे यानी प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा पास करके मजिस्ट्रेट बन सकता है। जो लोग परीक्षा देकर मजिस्ट्रेट बनते हैं वे कुछ वर्षों के लिए द्वितीय/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट रहते हैं, फिर उन्हें पदोन्नत किया जाता है।
न्यायालय में दो प्रकार के मामले होते हैं
मजिस्ट्रेट और जज के बीच अंतर जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि कोर्ट में मोटे तौर पर दो प्रकार के मामले होते हैं, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। दीवानी मामले ऐसे मामले हैं जिनमें अधिकार और मुआवजे की मांग की जाती है। ऐसे अन्य आपराधिक मामले हैं जिनमें सजा की मांग की जाती है।
मजिस्ट्रेट और जज के बीच का अंतर जानें
मजिस्ट्रेट और जज के बीच रैंक और अधिकार का अंतर होता है। एक मजिस्ट्रेट मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेट के स्तर में भी कई स्तर होते हैं।
इनमें सबसे ऊपर का पद CJM यानी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का होता है (धारा 12 सीआरपीसी)। महानगरों में इसे मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट (धारा 17) भी कहा जाता है। जिले में एक सीजेएम होता है।
जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन की निगरानी करना, भू-राजस्व एकत्र करना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता है। डीएम भूमि के पंजीकरण, खेती के खेतों के विभाजन, विवादों के निपटारे, दिवालिया होने, जागीरों के प्रबंधन, किसानों को ऋण देने और सूखा राहत के लिए भी जिम्मेदार हैं।
जिले के अन्य सभी अधिकारी उनके अधीनस्थ थे और उन्हें अपने-अपने विभागों की हर गतिविधि उपलब्ध कराते थे। उन्हें जिलाधिकारी के कार्य भी सौंपे गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वह जिले की पुलिस और अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी कर सकता है।
जज सीजेएम से ऊपर होते हैं। जिला जज और एडीजे यानी अतिरिक्त जिला जज (धारा 9 और 10) के जज के पद में आते हैं। इस स्तर पर, जब जज दीवानी मामलों से निपटते हैं, तो उन्हें जिला जज कहा जाता है, लेकिन जब वही जज आपराधिक मामलों से निपटते हैं, तो उन्हें सत्र जज कहा जाता है। दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करने वाला एक ही जज होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
मजिस्ट्रेट और जजों का पदानुक्रम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 12): यह किसी भी जिले में मजिस्ट्रेट का सर्वोच्च पद है। जिले के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दे सकता। वे ऐसी सजा नहीं दे सकते जो 7 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास तक हो।
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सीआरपीसी की धारा 11): ये मजिस्ट्रेट किसी भी मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं। कोई भी मामला शुरू में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास जाता है। यह न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी अभियुक्त को उनके न्यायालय में दोषी ठहराया जाता है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपराध के लिए तीन वर्ष तक की कैद और दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट तीन साल से अधिक कारावास और दस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है।
मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (सीआरपीसी की धारा 11): इस पद से न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट का आदेश शुरू होता है। दीवानी से जुड़ा कोई भी मामला इस कोर्ट में सबसे पहले आता है। आपराधिक मामलों में, एक द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना या इन दोनों को एक साथ किसी भी दोषी को साबित कर सकती है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 16) : जबकि महानगरों के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसे पद रखे गए हैं. इन पदों पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को रखा गया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 20): इसके अलावा, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और महानगर में जितने चाहें उतने कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है।
सजा देने की शक्ति
सत्र न्यायाधीश(सीआरपीसी की धारा 28): सत्र न्यायालय (सत्र न्यायालय) की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जज द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय अतिरिक्त और साथ ही सहायक सत्र जजों की नियुक्ति करता है। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं। लेकिन अगर मौत की सजा दी जाती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा इस सजा की पुष्टि अनिवार्य है।
अतिरिक्त/सहायक सत्र न्यायाधीश (सीआरपीसी की धारा 28): इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। वे सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हत्या, चोरी, डकैती, जेबकतरे और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। एक सहायक सत्र न्यायाधीश मौत की सजा या आजीवन कारावास या दस साल से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 29): सीजेएम मौत की सजा या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है।
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 29): वह तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास की सजा, या दस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, या दोनों की सजा दे सकता है।
द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 29): वह एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, या दोनों की सजा दे सकता है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 29): सीएमएम के पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होंगी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीआरपीसी की धारा 29): उसके पास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ हैं।