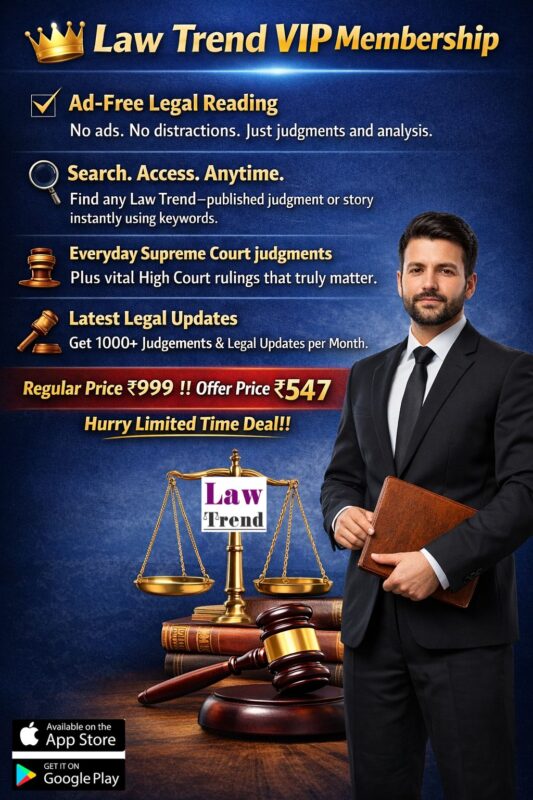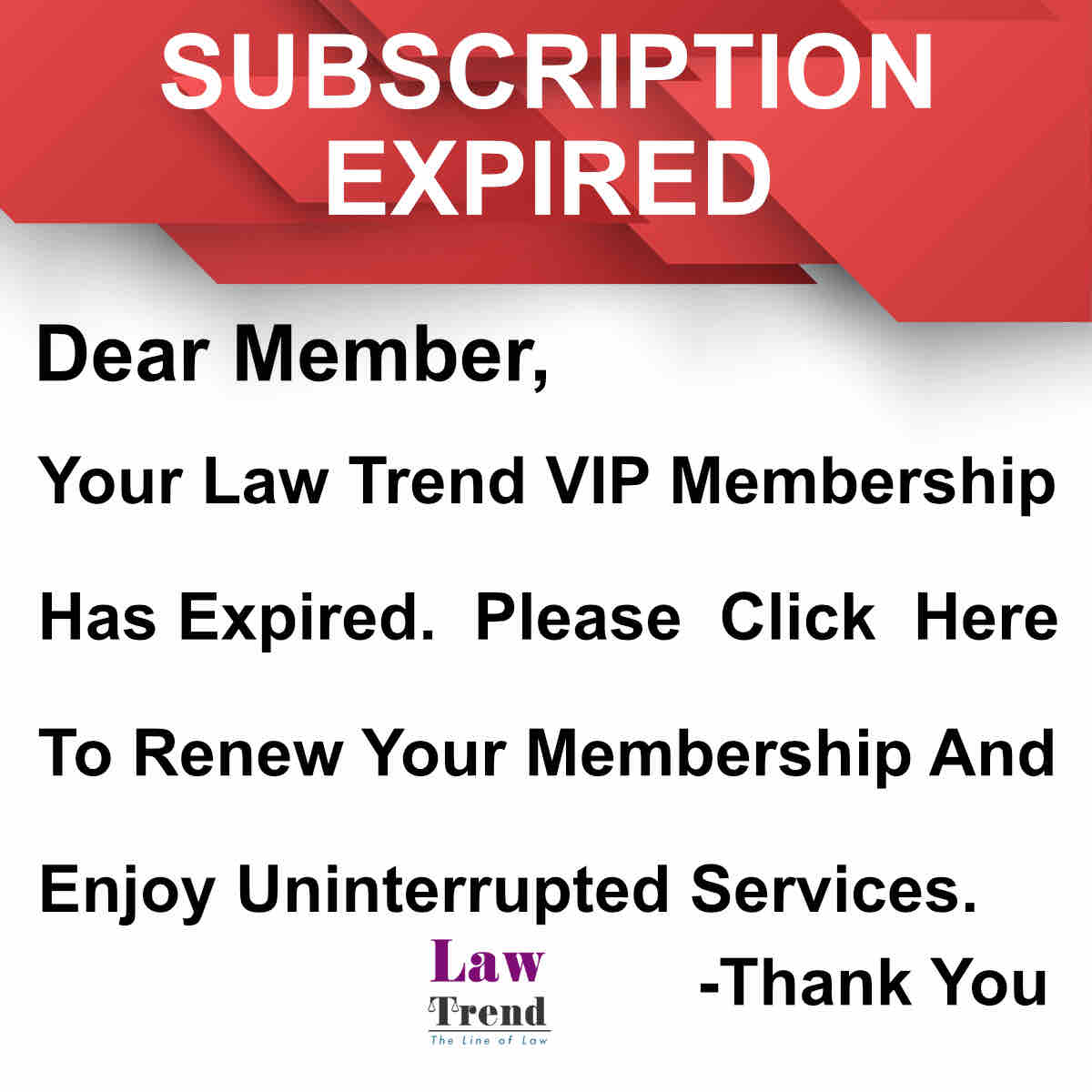सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि यह सिद्धांत कि अदालतें कानून नहीं बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं, एक मिथक है जो “बहुत पहले ही फूट चुका है”।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कहा क्योंकि उसने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता शामिल होंगे। लोकसभा और CJI, “चुनाव की शुद्धता” बनाए रखने के लिए।
जस्टिस जोसेफ ने फैसले को लिखते हुए उदाहरण दिया, जहां शीर्ष अदालत ने निर्देश देने का सहारा लिया था, जो कानून का रंग था, अगर कानून में कोई शून्य था या कोई कानून नहीं था।
निर्णय ने संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया।
इसने जोर देकर कहा कि जब कोई अदालत किसी कानून या संशोधन को असंवैधानिक घोषित करती है, तो उस पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने या संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
“उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उन्हें दी गई शक्ति के तहत नियम बनाते हैं। निस्संदेह, वे विधानमंडल के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में शक्ति का प्रयोग विधायी प्रकृति का होगा।”
“जब कार्यपालिका, यानी भारत संघ द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश बनाया जाता है, तो यह कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग करने का मामला है। जब संसद किसी व्यक्ति को अपनी अवमानना का दोषी ठहराती है और उसे दंडित करती है, तो कार्यवाही सूचित की जाती है। न्यायिक शक्ति की विशेषता से,” यह कहा।
फैसले में कहा गया, “यह सिद्धांत कि अदालतें कानून नहीं बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं, एक मिथक है जो बहुत पहले ही फूट चुका है।”
इसने कहा कि भारत में “सख्त सीमांकन या शक्तियों का पृथक्करण” नहीं था क्योंकि विधायिका और न्यायपालिका लोकतंत्र में अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती रही हैं।
उदाहरण देते हुए, निर्णय ने कहा कि जब संसद किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए बुलाती है और दंडित करती है तो वह न्यायपालिका की भूमिका निभा रही है।
“यह सच हो सकता है कि अदालतों का सहारा समाज में सभी बीमारियों का इलाज नहीं है … हम समान रूप से जानते हैं कि अदालतों को सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ही सम्राटों की तरह व्यवहार करना चाहिए,” यह कहा।
इसने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
“समान रूप से, न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का एक हिस्सा बनाने के रूप में मान्यता दी गई है। कानून की न्यायिक समीक्षा संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है,” इसने कहा, “एक अदालत जब यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की घोषणा करती है असंवैधानिक, यदि ऐसा है कि, यह अपनी सीमा के भीतर है, तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।”
अदालत की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से निपटते हुए, इसने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी असंवैधानिक घोषित करना उसकी शक्तियों का एक हिस्सा है।
“शायद अधिकांश देशों के विपरीत, भारत में मूल संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादन के मद्देनजर, यहां तक कि संविधान में संशोधन को भी अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस तरह की कवायद अदालत को इस आरोप के सामने नहीं ला सकती है कि वह सीमाओं का पालन नहीं कर रही है।” संविधान द्वारा निर्धारित, “यह कहा।
एक अंतिम विश्लेषण में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक स्रोत में अतिरिक्त शक्ति की धारणा से बहने वाली शक्ति के अत्याचार को रोकने के लिए है।
“न्यायिक सक्रियता, हालांकि, एक ठोस न्यायिक आधार होना चाहिए और व्यक्तिवाद के एक मात्र अभ्यास में पतित नहीं हो सकता है,” यह कहा।