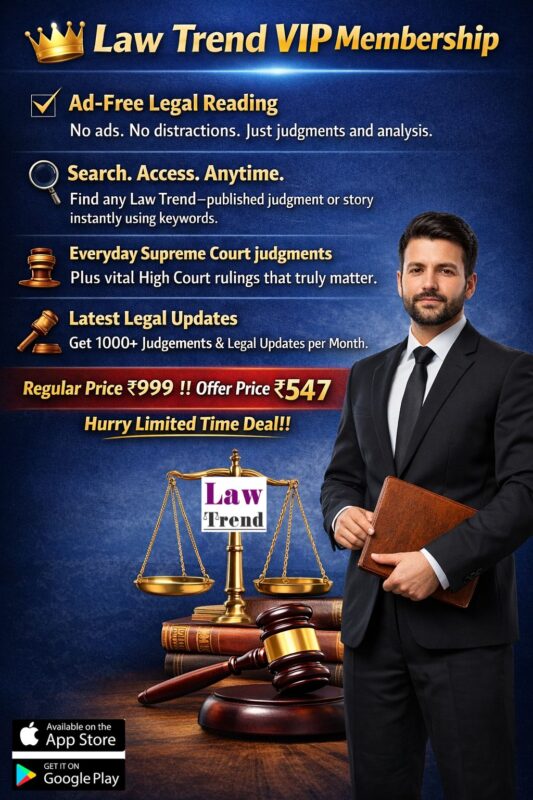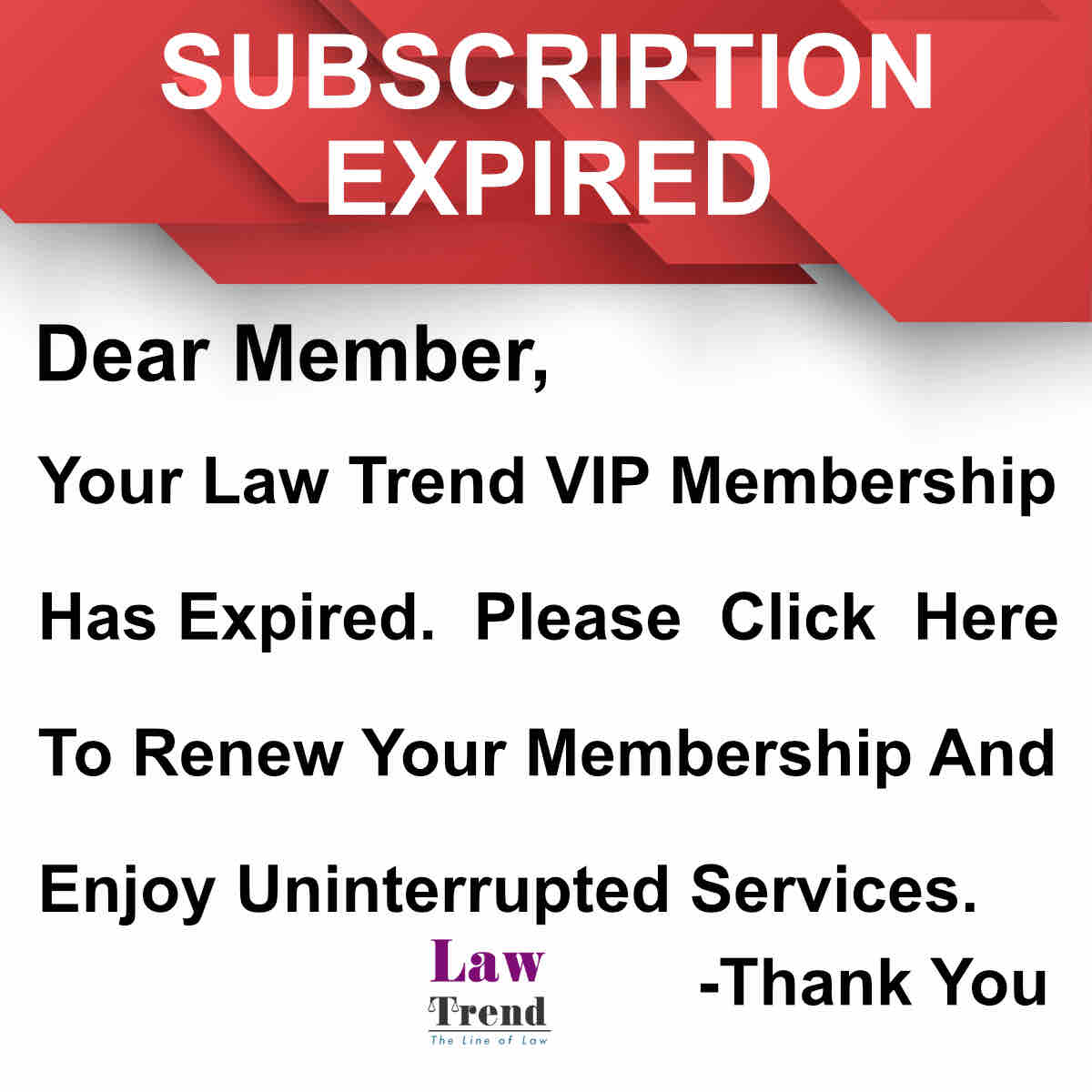सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूरे भारत में प्रवेश स्तर के न्यायिक अधिकारियों के कैरियर की धीमी और असमान प्रगति से निपटने के लिए उनकी वरिष्ठता (seniority) तय करने के मानदंडों में “कुछ हद तक राष्ट्रव्यापी एकरूपता” की आवश्यकता है।
हालांकि, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका हाईकोर्ट (High Court) की शक्तियों में अतिक्रमण करने का दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं है। पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जयमाल्य बागची भी शामिल हैं, उच्च न्यायिक सेवा (HJS) कैडर में वरिष्ठता निर्धारण के लिए एक समान, राष्ट्रव्यापी मानदंड तैयार करने पर विचार कर रही है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मुद्दा ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (AIJA) द्वारा 1989 में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ था। 7 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने देश भर में निचले न्यायिक अधिकारियों द्वारा सामना किए जा रहे कैरियर में ठहराव से संबंधित मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया था।
मंगलवार को, पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की और इस बात पर चिंता व्यक्त की कि धीमी प्रगति के कारण प्रतिभाशाली युवा वकील न्यायिक सेवा में शामिल होने से हिचक रहे हैं। अदालत ने इस स्थिति पर ध्यान दिया कि “अधिकांश राज्यों में, सिविल जज (CJ) के रूप में भर्ती न्यायिक अधिकारी अक्सर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (PDJ) के स्तर तक नहीं पहुँच पाते, हाईकोर्ट जज के पद तक पहुँचना तो दूर की बात है।”
14 अक्टूबर को, पीठ ने विचार के लिए मुख्य प्रश्न तैयार किया था: “उच्च न्यायिक सेवाओं के कैडर में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए”। इसने यह भी स्पष्ट किया था कि मुख्य मुद्दे की सुनवाई करते हुए, यह “अन्य सहायक या संबंधित मुद्दों” पर भी विचार कर सकती है।
समान ढांचे के खिलाफ दलीलें
सुनवाई के दूसरे दिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने शीर्ष अदालत को एक समान वरिष्ठता ढांचा लागू करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला हाईकोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो “संवैधानिक रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए सशक्त” हैं।
श्री द्विवेदी ने दलील दी, “हाईकोर्ट अपने राज्यों के भीतर के तथ्यों और मौजूदा स्थितियों से वाकिफ हैं। वे वरिष्ठता और पदोन्नति के मुद्दे से निपटने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं… यह हाईकोर्ट को मजबूत करने का समय है, उन्हें कमजोर करने का नहीं।”
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्याय मित्र (amicus curiae) द्वारा प्रस्तुत डेटा “अधूरा, और पहले से मौजूद कानूनी स्थितियों पर आधारित” था, और इसलिए विभिन्न राज्यों की जमीनी हकीकतों को नहीं दर्शाता। उन्होंने आग्रह किया, “अगर स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग है, तो कोई भी समान कोटा या नियम असंतुलन पैदा करेगा… हाईकोर्ट को अपनी परिस्थितियों से निपटने दें।”
श्री द्विवेदी ने मौजूदा सेवा नियमों में भिन्नता पर भी प्रकाश डाला, यह तर्क देते हुए कि एक समान कोटा लागू करने का कोई भी प्रयास पदोन्नत (promotee) और सीधी भर्ती (direct recruit) वाले न्यायिक अधिकारियों के बीच “नाजुक संतुलन को बिगाड़” सकता है।
अदालत की टिप्पणियां और स्पष्टीकरण
हालांकि, पीठ ने हाईकोर्ट के अधिकार का सम्मान करते हुए निरंतरता की आवश्यकता पर बल दिया। CJI ने टिप्पणी की, “हाईकोर्ट के बीच कुछ एकरूपता होनी चाहिए… हम नामों की सिफारिश करने के लिए हाईकोर्ट के विवेक को नहीं छीनेंगे। लेकिन हर हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग नीतियां क्यों होनी चाहिए?”
श्री द्विवेदी को आश्वासन देते हुए, CJI ने कहा, “हम अप्रत्यक्ष रूप से या दूर से भी हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्तियों को छीनने का इरादा नहीं रखते हैं।”
जस्टिस सूर्य कांत ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि पीठ का ध्यान सामान्य सिद्धांतों पर था, न कि व्यक्तिगत विवादों पर। जस्टिस कांत ने कहा, “व्यक्तिगत वरिष्ठता विवादों पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह एक व्यापक, मार्गदर्शक ढांचा होने जा रहा है।” CJI ने कहा कि यह अभ्यास स्थिति को सुधारने के लिए “ट्रायल एंड एरर” (trial and error) पद्धति के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
न्याय मित्र की दलीलें
अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर (न्याय मित्र) ने कैरियर में ठहराव के एक प्रमुख कारक पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अधिकांश राज्यों में पदोन्नति “योग्यता (merit) से अधिक वरिष्ठता (seniority) से प्रेरित” थी, जिसका मुख्य कारण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACRs) के मूल्यांकन का तरीका था।
श्री भटनागर ने समझाया, “पदोन्नत जज, अधिक उम्र के होने के कारण, अक्सर अगले पदोन्नति चरण तक पहुंचने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। नतीजतन, कैडर के शीर्ष पर आमतौर पर सीधी भर्ती वाले काबिज होते हैं, जो छोटे होते हैं और इसलिए लंबे समय तक पात्र बने रहते हैं।” उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देते हुए प्रस्ताव दिया कि जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए हर 30 विचाराधीन नामों में से 15 पदोन्नत जजों और 15 सीधी भर्ती वालों में से होने चाहिए।
मामले की सुनवाई बेनतीजा रही और आगे भी जारी रहेगी।