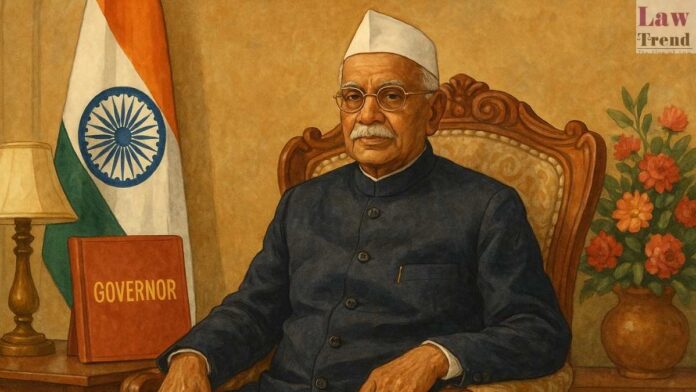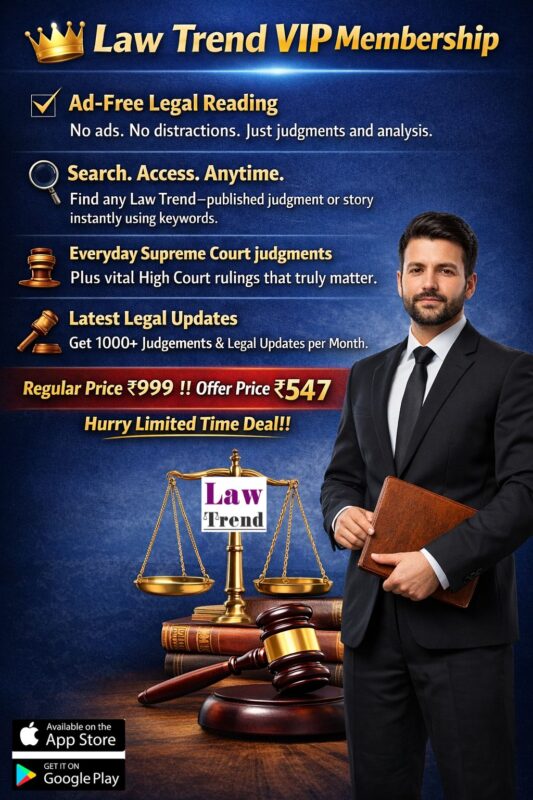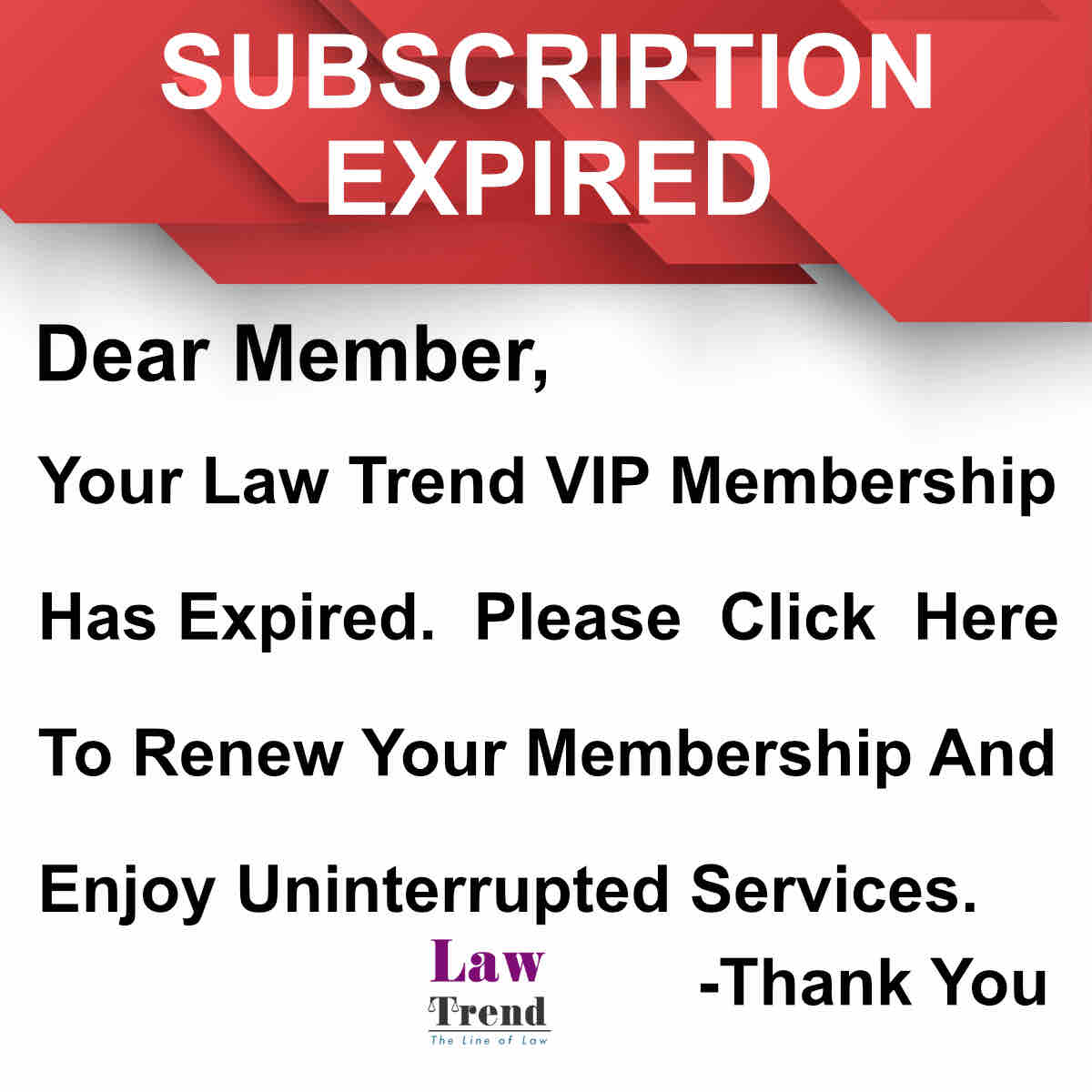राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन, बहुत कम संवैधानिक पद ऐसे हैं जो राज्यपाल के पद की तरह लगातार विवादों में घिरे रहे हों। दशकों से राजनीतिक और कानूनी बहसों का केंद्र यही सवाल रहा है कि क्या राज्यपाल राज्य के एक निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक के रूप में काम करते हैं, या उन्हें नियुक्त करने वाली केंद्र सरकार के एक राजनीतिक एजेंट के रूप में? यह टकराव किसी की राय या पक्षपात का मामला नहीं है, बल्कि यह उस संवैधानिक ढांचे में ही मौजूद है जो राज्यपाल की दोहरी और अक्सर विरोधाभासी जिम्मेदारियों को तय करता है।
संवैधानिक जिम्मेदारी: एक पद, दोहरी भूमिका
भारत का संविधान कई प्रमुख अनुच्छेदों के माध्यम से राज्यपाल की स्थिति को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति उन्हें सौंपता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 155) और वे “राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत” पद पर बने रहते हैं (अनुच्छेद 156), जिसका व्यावहारिक अर्थ केंद्र सरकार की इच्छा तक होता है।
एक तरफ, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में “सहायता और सलाह” देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। इस भूमिका में, राज्यपाल से यह उम्मीद की जाती है कि वे भारत के राष्ट्रपति की तरह एक नाममात्र के प्रमुख के रूप में काम करेंगे, जो चुनी हुई राज्य सरकार की सलाह से बंधे हों। उनके कार्यों में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना (अनुच्छेद 164), राज्य विधानमंडल को बुलाना और भंग करना (अनुच्छेद 174), और विधेयकों पर सहमति देना (अनुच्छेद 200) शामिल है।
दूसरी ओर, संविधान अनुच्छेद 163 में ही एक महत्वपूर्ण अपवाद भी देता है। इसके अनुसार, राज्यपाल उन कार्यों के लिए मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार उन्हें अपने “विवेक” से करना है। यही विवेकाधीन शक्ति, केंद्र के हाथ में नियुक्ति और हटाने की शक्ति के साथ मिलकर, राज्यपाल की दूसरी भूमिका बनाती है – केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि और एजेंट की भूमिका।
विवाद के मुख्य बिंदु
इन दोनों भूमिकाओं के बीच का टकराव उन विशेष स्थितियों में सबसे ज़्यादा सामने आता है जहाँ राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति: जब चुनाव में किसी एक पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, यह तय करने में राज्यपाल के विवेक की भूमिका सामने आती है। इस फैसले की अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित होने के लिए आलोचना की जाती है। राज्यपालों पर अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल से जुड़ी पार्टियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया जाता है, भले ही उनके पास बहुमत का स्पष्ट दावा न हो।
- राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356): यदि राज्यपाल को लगता है कि “ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है,” तो वे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। यह रिपोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकती है। ऐतिहासिक रूप से, यह सबसे विवादास्पद शक्ति रही है। आंकड़े बताते हैं कि अनुच्छेद 356 का 100 से अधिक बार उपयोग किया गया है, और अक्सर ऐसे कारणों पर जो पक्षपातपूर्ण और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने या बर्खास्त करने के उद्देश्य से प्रेरित थे।
- विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना: अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों में देरी करने या उन्हें वीटो करने के लिए किया गया है, खासकर जब राज्य और केंद्र में अलग-अलग दलों की सरकारें हों।
न्यायपालिका का हस्तक्षेप और संवैधानिक सीमाएं
न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करने और एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए बार-बार हस्तक्षेप किया है।
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) मामले में, कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्हें अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से उन्हें अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है।
- सबसे महत्वपूर्ण फैसला ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश निर्धारित किए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय में। इस फैसले ने स्थापित किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
- हाल ही में, नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को और सीमित करते हुए कहा कि राज्यपाल विधानसभा को इस तरह से नहीं बुला सकते या भंग नहीं कर सकते जिससे एक चुनी हुई सरकार को कमजोर किया जा सके।
सुधारों का अधूरा एजेंडा
इस लगातार टकराव को पहचानते हुए, कई उच्च-स्तरीय आयोगों ने राज्यपाल के पद को राजनीतिक दबावों से बचाने के लिए सुधारों की सिफारिश की है।
- सरकारिया आयोग (1988) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, राज्य के बाहर का होना चाहिए, और हाल ही में सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया होना चाहिए। साथ ही, उनकी नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए।
- पुंछी आयोग (2010) ने इन सुझावों को दोहराया और आगे बढ़कर राज्यपालों के लिए पांच साल का निश्चित कार्यकाल प्रस्तावित किया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उन्हें केवल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति की “इच्छा” पर।
निष्कर्ष: एक ढांचागत दुविधा
राज्यपाल की भूमिका पर बहस केवल व्यक्तियों के आचरण के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के भीतर एक मौलिक ढांचागत दुविधा के बारे में है। इस पद की कल्पना राज्यों के भीतर संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने और साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए की गई थी। हालांकि, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, अस्पष्ट रूप से परिभाषित विवेकाधीन शक्तियों के साथ मिलकर, इस पद को राजनीतिक हेरफेर के प्रति संवेदनशील बनाती है।
जब तक एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित नहीं होती जहाँ केंद्र सरकार संयम बरते और राजभवनों में बैठे लोग “संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव” की अपनी शपथ को सबसे ऊपर रखें, तब तक राज्यपाल का पद एक विवादित क्षेत्र बना रहेगा।
लेखक: सौरभ यादव
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं।