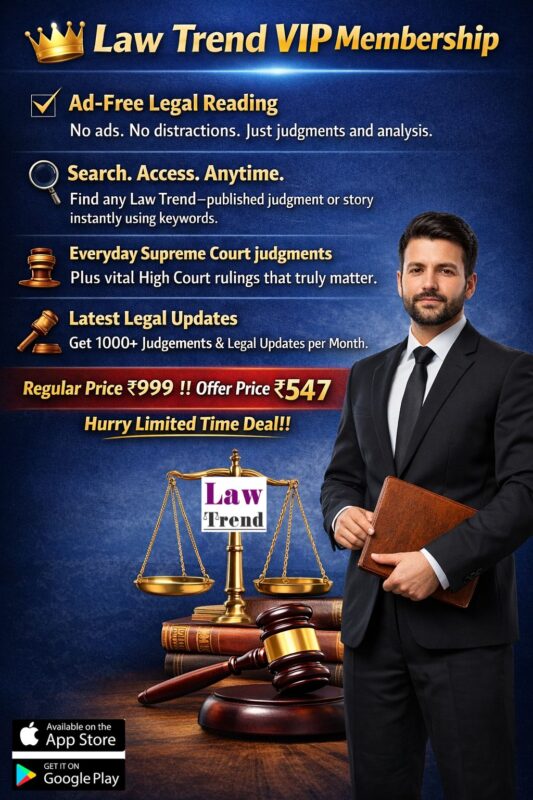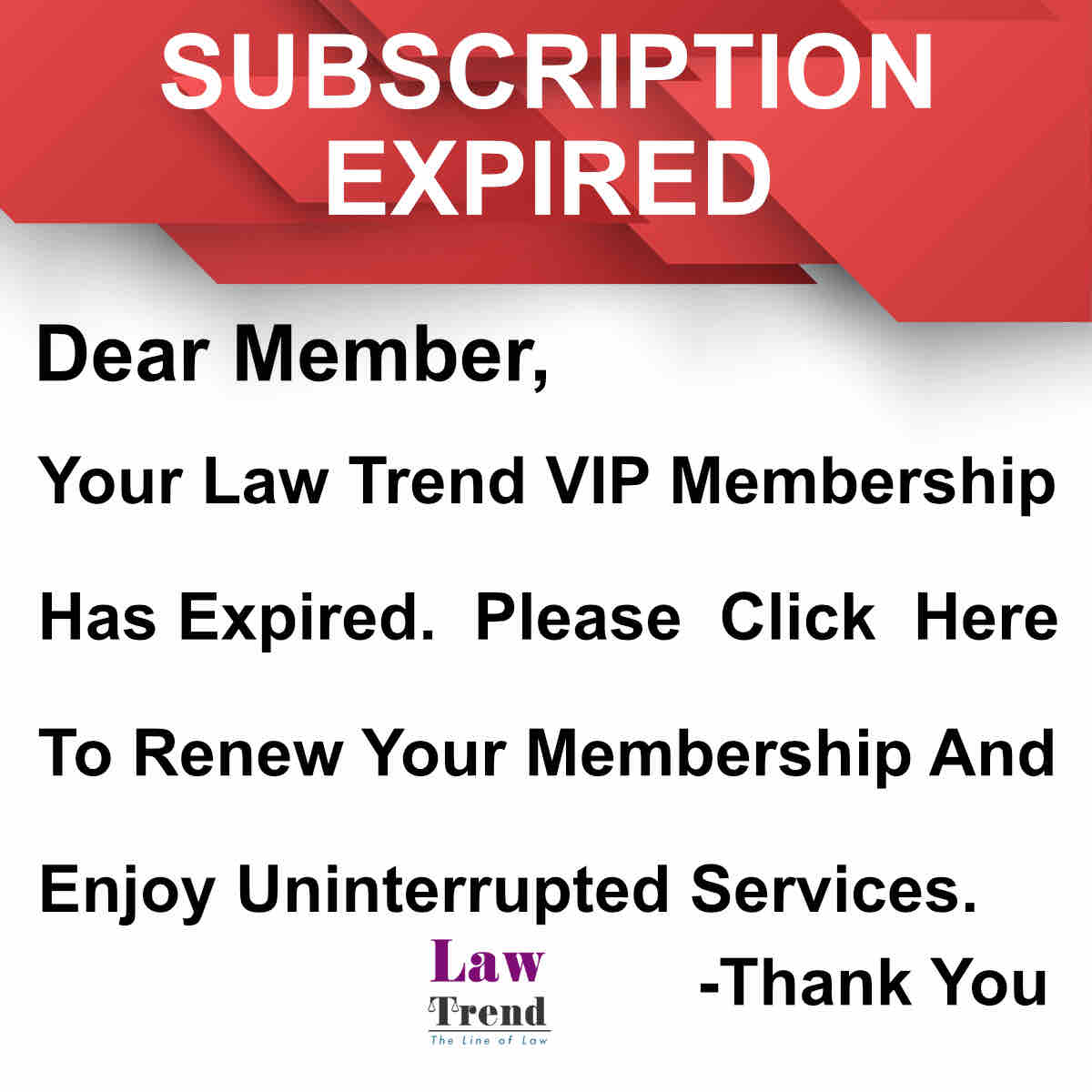सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने रविवार को कहा कि डीपफेक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, के यौन शोषण से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत कानून बनाने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेजी से विकसित होती तकनीक बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श “बालिका की सुरक्षा: भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की दिशा में” के समापन सत्र में बोल रही थीं। इस कार्यक्रम का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस समिति ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से किया था।
“तेजी से विकसित होती तकनीक से पैदा होने वाले खतरे ‘तलवार की धार पर लटके’ खतरे जैसे प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ में, डीपफेक्स और एआई-सक्षम बाल शोषण पर कानून बनाना, बाल यौन शोषण सामग्री की 24 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य करना, प्लेटफॉर्म-स्तर पर आयु सत्यापन लागू करना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया समय की निगरानी करना समय की मांग है,” उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति नागरत्ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस समिति की अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि शीर्ष अदालत एक “एआई साइबर अपराध परामर्श समिति (बालिका)” गठित करने पर विचार कर सकती है, जो यह अध्ययन करेगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकें बालिकाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं और इनसे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं।
उन्होंने न्यायपालिका में एआई से जुड़े खतरों और चुनौतियों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि पर्याप्त सतर्कता से हम हिंसा और बाल तस्करी जैसी घटनाओं को पहले ही रोक सकते हैं। उन्होंने महिला भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त प्रवर्तन की जरूरत पर भी जोर दिया।
“कानून अपने आप समाज को नहीं बदल सकता। हमें भावी माता-पिता में बालिकाओं के अवसरों और संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि ‘लड़की बोझ है’ जैसी धारणाएं समाप्त हों,” उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बालिकाओं के सशक्तिकरण को पोषण और शिक्षा तक पहुंच से जोड़ा। उन्होंने स्कूलों में पोषण साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने, एचएफएसएस (उच्च वसा, शर्करा और नमक) खाद्य पदार्थों की राष्ट्रीय परिभाषा तय करने, पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने, अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर टैक्स लगाने और स्कूलों के आसपास जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लागू करने की बात कही।
“एक बालिका को बचाना, एक पीढ़ी को बचाना है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने शिक्षा को बालिका के लिए सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, अधिकारों के प्रति जागरूकता आती है और सामाजिक बुराइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। उन्होंने हिंसा, तस्करी, बाल विवाह या अन्य सामाजिक बुराइयों से प्रभावित बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए व्यवस्थित मार्ग तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बाल तस्करी से निपटने के लिए फॉरेंसिक और वित्तीय ट्रेसिंग के जरिए पेशेवर जांच करने और पुनर्वास को राज्य का दायित्व बनाते हुए उसे मापने योग्य परिणामों से जोड़ने की सिफारिश की।
उन्होंने ज़ोर दिया कि हर ज़िले में बाल और लैंगिक संवेदनशील चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
बाल विवाह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोकथाम और प्रतिक्रिया के प्रयास समुदाय स्तर पर पंचायतों, स्थानीय समुदायों और अधिकारियों की भागीदारी से ही सबसे प्रभावी हो सकते हैं, न कि अलग-अलग विभागों के एकांगी प्रयासों से।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने संवेदनशील पुलिस प्रशिक्षण और न्यायिक प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने, विभागों के बीच नियमित समन्वय सुनिश्चित करने और पीड़ित संतुष्टि एवं सजा दरों की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि बच्चों के लिए संवेदनशील न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने लिंग चयन में तकनीकी दुरुपयोग, कानूनी अस्पष्टताओं और प्रवर्तन में कमियों से निपटने के लिए ठोस निगरानी तंत्र स्थापित करने की भी बात कही।
“डेटा एक मूल्यवान संसाधन है और हमें सटीक आंकड़े एकत्र करने और प्रकाशित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही वे तस्वीर नकारात्मक दिखाएं,” उन्होंने कहा।
अपने संबोधन के अंत में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि बालिका सशक्तिकरण एक अधिक न्यायपूर्ण और समानता-आधारित समाज की रचना की आधारशिला है। उन्होंने यह भी कहा कि हाशिये पर रहने वाले समुदायों, विकलांग बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को संविधान और अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संधियों के अनुरूप विशेष मान्यता और सहयोग मिलना चाहिए।
“हमें नियमित रूप से आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर लिंगानुपात में सुधार हो रहा है या नहीं,” उन्होंने कहा।