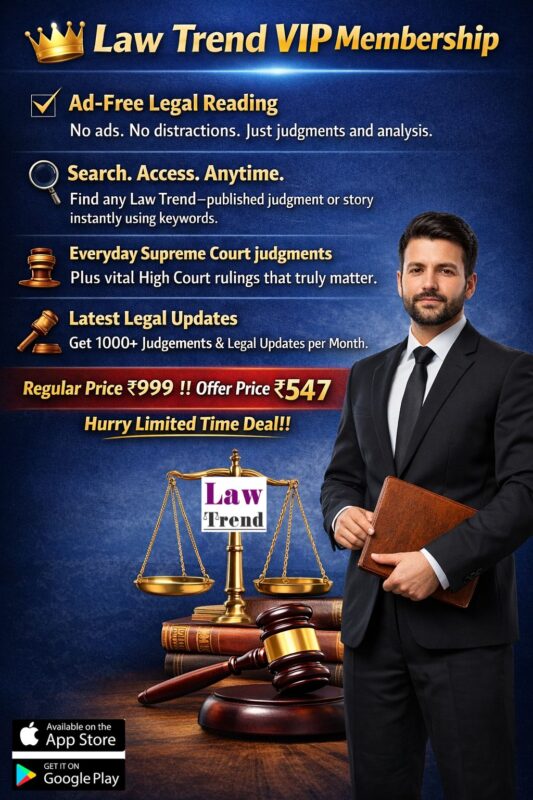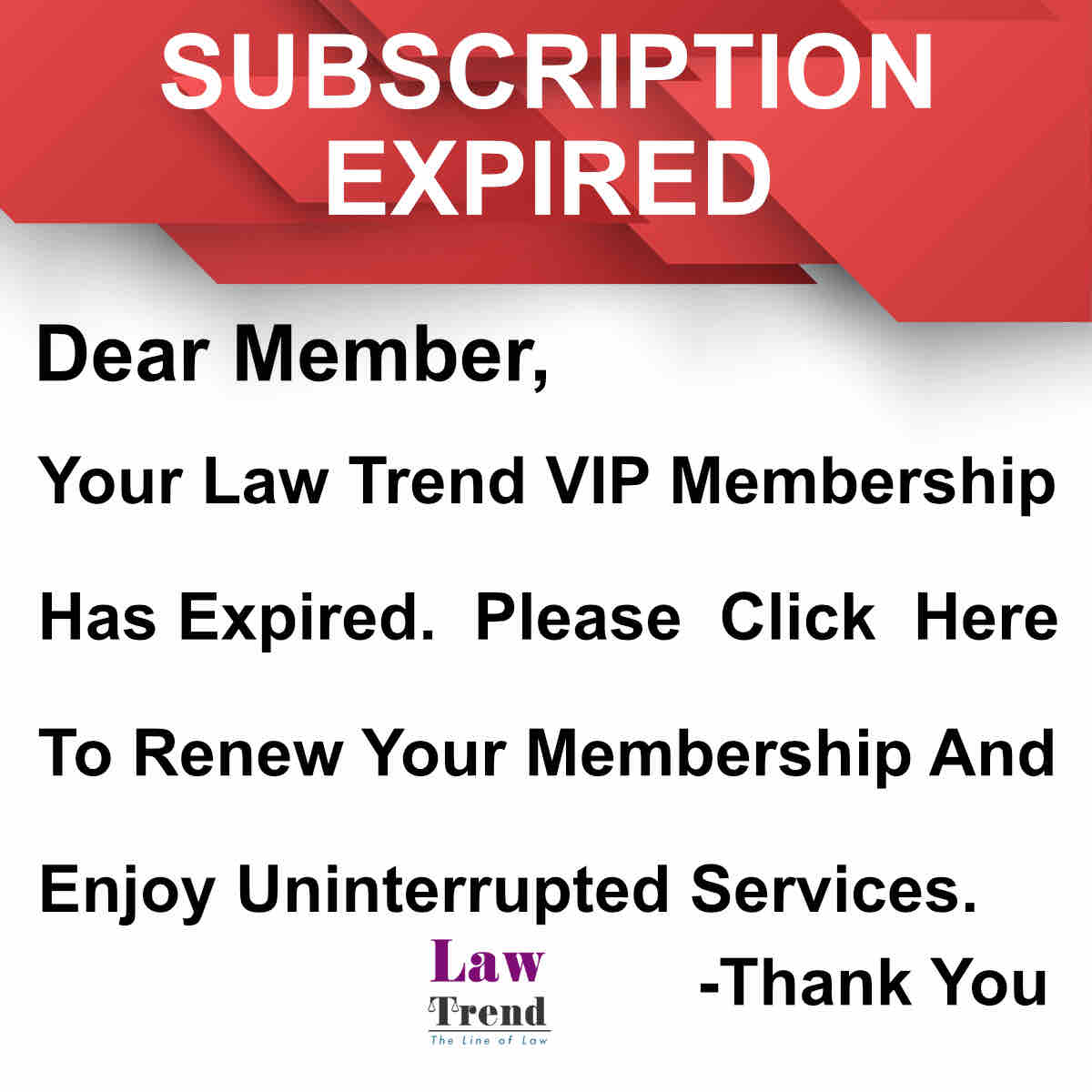भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने बुधवार को कहा कि विधि शिक्षा का उद्देश्य केवल बार और बेंच के लिए पेशेवर तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों को गढ़ना है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति समर्पित हों।
‘लीगल एंड जस्टिस एजुकेशन @2047: एन एजेंडा फॉर 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस’ विषय पर आयोजित पहले प्रोफेसर (डॉ.) एन.आर. माधव मेनन स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कानून और न्याय तक पहुंच कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार न होकर प्रत्येक नागरिक की सजीव वास्तविकता बननी चाहिए।
सीजेआई गवई ने कहा कि लंबे समय से भौगोलिक, आर्थिक और भाषायी बाधाएं वंचित व कमजोर नागरिकों को न्याय से दूर रख रही हैं। “आर्थिक विषमता का अर्थ यह है कि कानूनी उपचार उपलब्ध होने पर भी वह उन तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि कानून वास्तव में सशक्तिकरण का साधन है तो इन बाधाओं को खत्म करना आवश्यक है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने तकनीक के माध्यम से शिक्षा का विस्तार करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने, कानूनी सहायता को मजबूत बनाने और प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता बताई।
सीजेआई ने यह भी कहा कि कानून स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक छात्र में संवैधानिक आदर्शों के प्रति गहरा सम्मान विकसित करें। साथ ही उन्होंने उभरते विधिक क्षेत्रों पर शोध संस्थान स्थापित करने पर जोर दिया।
सीजेआई ने पांच वर्षीय एकीकृत कानून कार्यक्रम और नेशनल लॉ स्कूल मॉडल की सफलता को स्वीकारते हुए कहा कि इसकी एक आलोचना यह है कि इसने अनजाने में अधिकांश स्नातकों को कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर मोड़ दिया है।
“कानूनी पेशेवर की असली शक्ति केवल कानून जानने में नहीं, बल्कि न्याय कायम रखने, लोकतंत्र की रक्षा करने और कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में डटे रहने में है,” उन्होंने कहा।
व्याख्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने विधि शिक्षा के तीन स्तंभ बताए—आधुनिकीकरण, नैतिकता और सबके लिए सुलभता।
उन्होंने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो कभी नवाचार और मेरिट की प्रतीक थीं, आज गंभीर फैकल्टी संकट का सामना कर रही हैं। वहीं, शिक्षा की ऊंची लागत के कारण यह केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक सीमित हो रही है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून की पढ़ाई को “आइवरी टॉवर” में नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक संघर्षों से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने डिजिटल-प्रथम शिक्षण पद्धति अपनाने, अंतर्विषयी शिक्षा को शामिल करने और प्रत्येक कानून स्कूल में कानूनी सहायता क्लीनिक अनिवार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
“आज की दुनिया में विधिक अभ्यास का हर पहलू तकनीक से जुड़ गया है, लेकिन हमारे कई लॉ स्कूल अब भी पुराने तौर-तरीकों से चिपके हुए हैं,” उन्होंने कहा।
सीजेआई गवई और जस्टिस सूर्यकांत दोनों का दृष्टिकोण एक था कि 2047 तक भारत की विधि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सुलभ, नैतिक, तकनीकी रूप से सशक्त और संवैधानिक आदर्शों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हो।