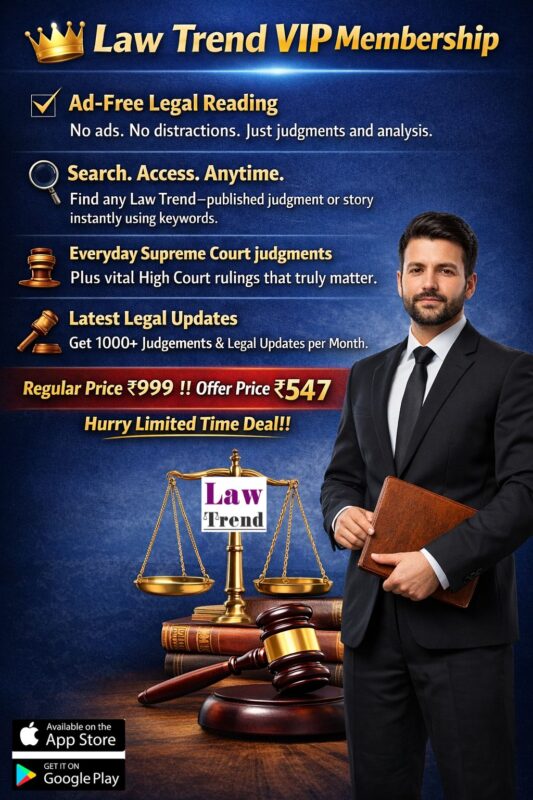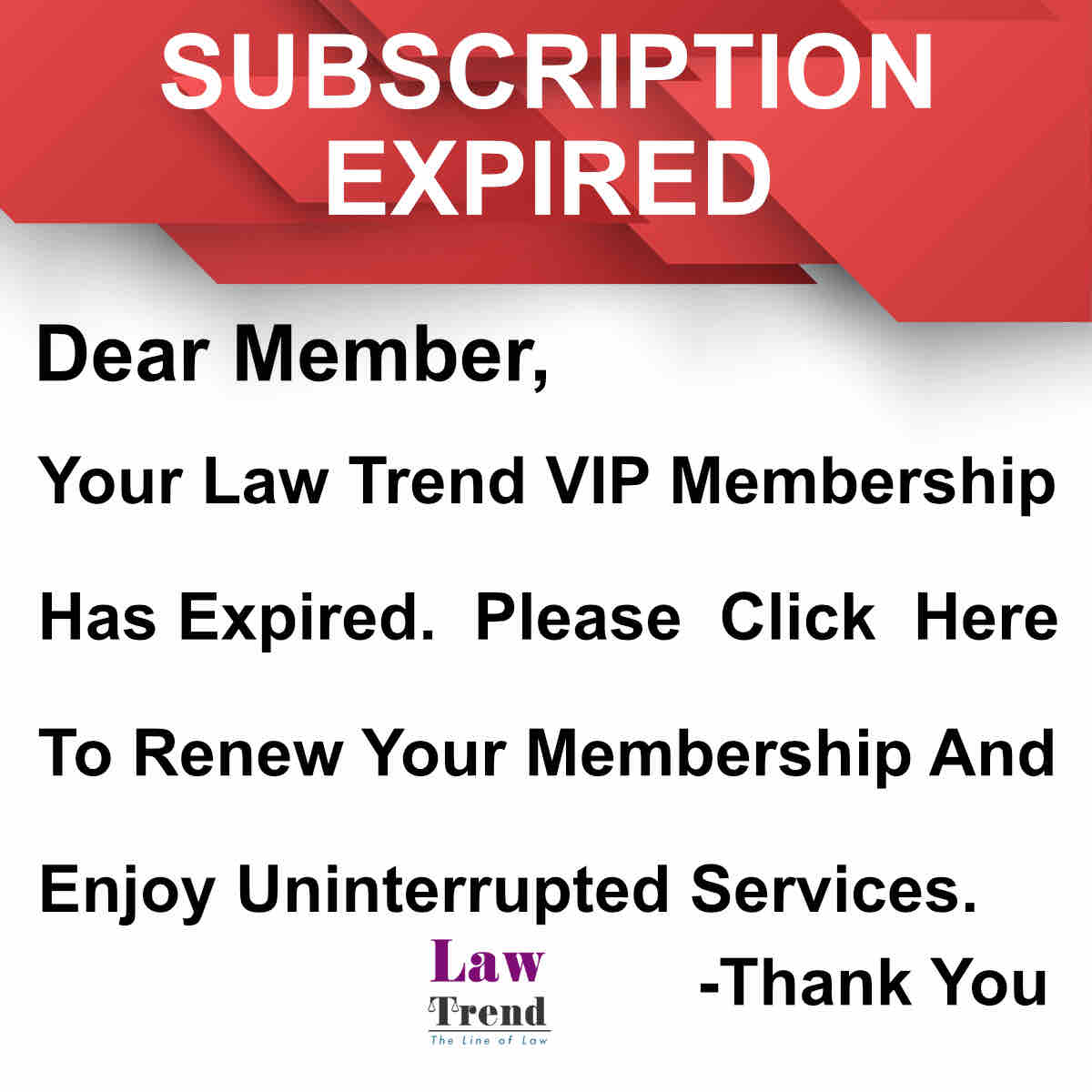सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने रविवार को चेतावनी दी कि बालिकाएं ऑनलाइन दुनिया में सबसे अधिक खतरे में हैं और भारत की मौजूदा जांच पद्धतियां जटिल साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केवल नीतिगत चर्चाओं और न्यायिक आदेशों से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित “बालिका की सुरक्षा: भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की दिशा में” राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के समापन सत्र में बोल रहे थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साढ़े तीन वर्षों में यह पहला कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे नियमित कानूनी विमर्श से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं कुछ शब्दों का आदमी हूं और जब कुछ कहना होता है तो घुमा-फिराकर नहीं कहता। साफ तौर पर कह दूं — सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा।”
उन्होंने कहा कि सैकड़ों परामर्श बैठकें और हैंडबुक जारी करने के बावजूद ये प्रयास तभी सार्थक होंगे जब काम ज़मीन पर किया जाए। “केवल न्यायिक फैसले पर्याप्त नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जमीनी स्तर पर काम करें। हमें ऐसे लोगों की टीम चाहिए जिनके दिल करुणा और संवेदना से भरे हों,” उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बताया कि परामर्श सत्र में साइबर अपराध पर चर्चा के दौरान डिजिटल दुनिया के अवसरों और खतरों दोनों पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने कहा, “बालिकाएं ऑनलाइन स्पेस में पीड़ित होने के अधिक खतरे में हैं। अपराधी डिजिटल दुनिया की गुमनामी, पहुंच और आपसी जुड़ाव का फायदा उठाकर महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। हमारी मौजूदा जांच पद्धतियां साइबर स्पेस में होने वाले जटिल अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम नहीं हैं।”
उन्होंने बाल सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा प्रावधान, कानून प्रवर्तन को मजबूत करने और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत की नीतिगत दृष्टि पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आज़ादी के बाद बच्चों के अधिकारों पर सामूहिक प्रयास देर से शुरू हुए। “इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे वोटर वर्ग का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए नीति निर्माताओं द्वारा अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि संविधान को 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी देश बाल अधिकारों, विशेषकर बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा में अभी भी जूझ रहा है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सामूहिक इच्छाशक्ति के चलते धीरे-धीरे प्रगति हो रही है।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा पर किसी भी चर्चा की शुरुआत समाज में गहराई से जड़ जमाए लैंगिक पूर्वाग्रह को स्वीकारने से होनी चाहिए। “हमें यह समझना होगा कि बालिकाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी जड़ें हमारे समाज के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में निहित हैं,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि बालिकाओं के हित में कई कानून और योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन सामाजिक सोच और परंपराओं के कारण बाधित होता है। “किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी, जहां हमें खुलकर और ईमानदारी से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को पहचानना और चुनौती देनी होगी,” उन्होंने कहा।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि वास्तविक परिवर्तन नीतिगत दस्तावेजों या अदालतों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन से शुरू होता है।
“वास्तविक बदलाव की शुरुआत सूक्ष्म स्तर पर, हमारे घरों में होनी चाहिए — बच्चों के साथ समान व्यवहार कर, जिम्मेदारियां समान रूप से बांटकर और बालिकाओं के अधिकारों व गरिमा का सम्मान कर। अगर हर घर समानता और सम्मान का स्थान बन जाए तो समाज अपने आप बदलेगा,” उन्होंने कहा।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के कई जनजातीय समुदायों, खासकर उत्तर-पूर्व में, बालिका के जन्म को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उत्सव की तरह मनाया जाता है — जिसे पूरे समाज को अपनाना चाहिए।