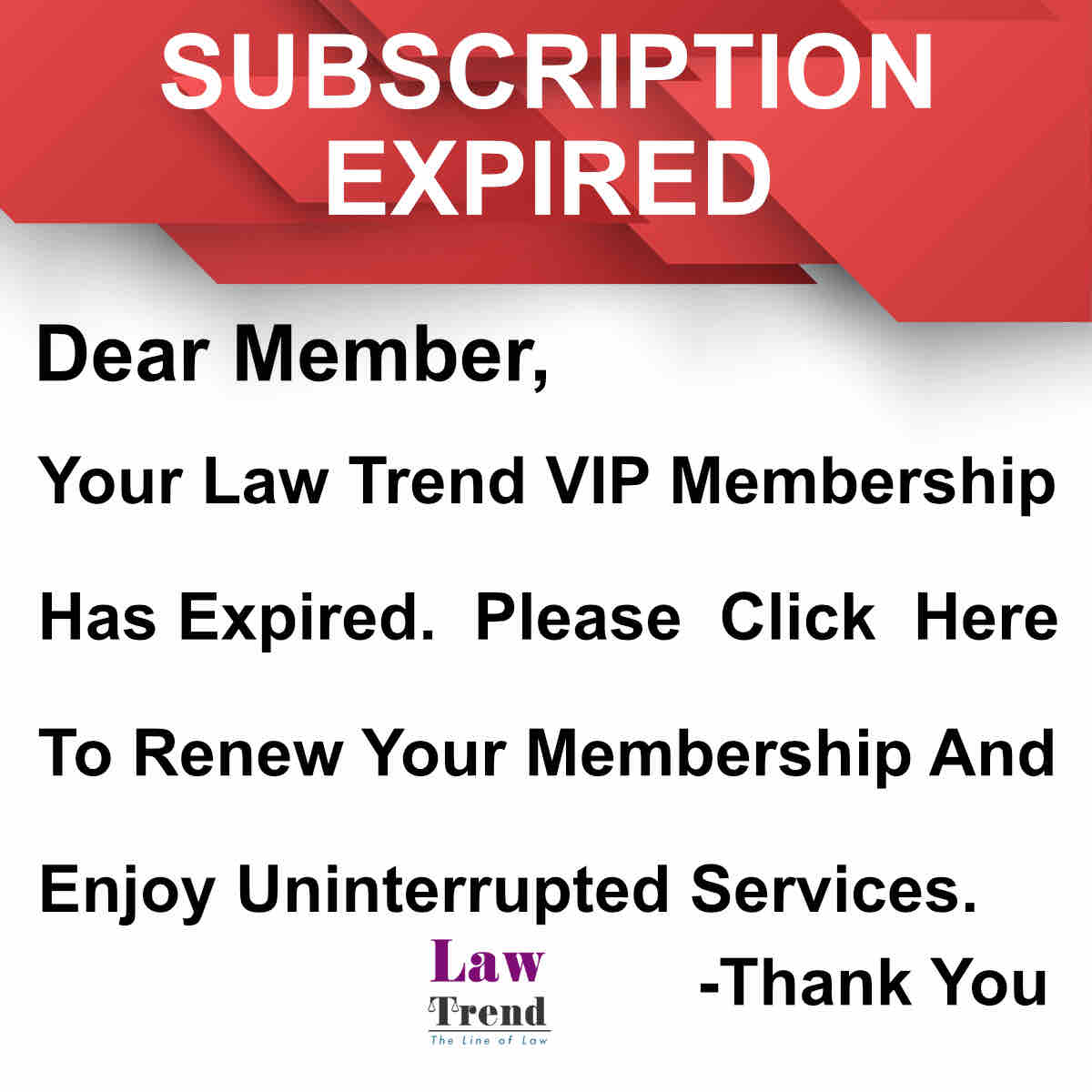दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी जिसमें संसद को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के उन प्रावधानों को समाप्त करे जो राज्य के विरुद्ध अपराधों और लोक शांति भंग करने से संबंधित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के पास न तो संसद को कानून बनाने का आदेश देने का अधिकार है और न ही उसे निरस्त करने का।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकार की राहत देना “न्यायपीठ द्वारा विधायन” के समान होगा, जो न्यायपालिका के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
“अधिनियम को समाप्त करना केवल संशोधन अधिनियम बनाकर ही संभव है। यह संसद का कार्य है। हम संसद को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते। यह विधायन होगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता,” अदालत ने कहा।
यह जनहित याचिका उपेंद्र नाथ दलई द्वारा दायर की गई थी, जिसमें बीएनएस की धाराओं 147 से 158 (राज्य के विरुद्ध अपराध) और धाराओं 189 से 197 (लोक व्यवस्था से संबंधित अपराध) को हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये प्रावधान सरकार को असहमति को दबाने और नागरिकों के समानता, जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की शक्ति देते हैं। उन्होंने इन धाराओं को “विपक्ष-मुक्त शासन” का उपकरण बताया और कहा कि ये संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हैं।
हालांकि, अदालत ने याचिका को अमान्य मानते हुए कहा,
“यदि हम याचिका की प्रार्थनाओं को देखें, तो स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संसद को एक संशोधन अधिनियम लाने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर नहीं दी जा सकतीं। अतः, याचिका खारिज की जाती है,” पीठ ने कहा।
कोर्ट पहले भी दलई द्वारा दायर ऐसी याचिकाओं पर चिंता जता चुकी है। मई में, अदालत ने बीएनएस को “क्रिमिनल एक्ट” कहने पर उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था,
“मज़ाक की भी एक सीमा होती है।”
गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), जो औपनिवेशिक कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेती है, 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। इसकी धाराएँ 147 से 158 राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, विघटनकारी गतिविधियों को उकसाने और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित हैं, जबकि धाराएँ 189 से 197 गैरकानूनी जमावड़ा, हिंसक दंगा और लोक व्यवस्था में विघटन जैसे अपराधों को दंडनीय बनाती हैं।
इस फैसले ने संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पुनः पुष्टि दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि कानून बनाना केवल संसद का अधिकार क्षेत्र है, न कि न्यायपालिका का।