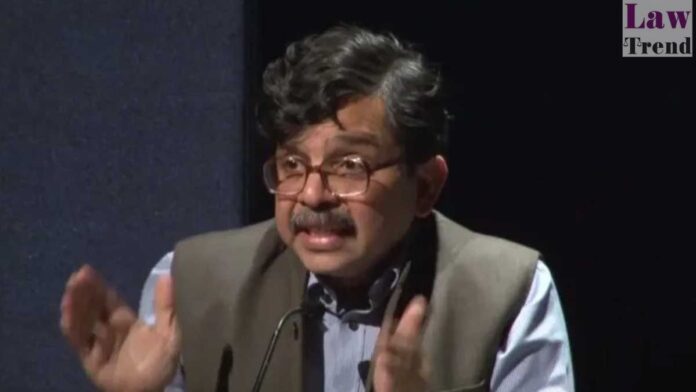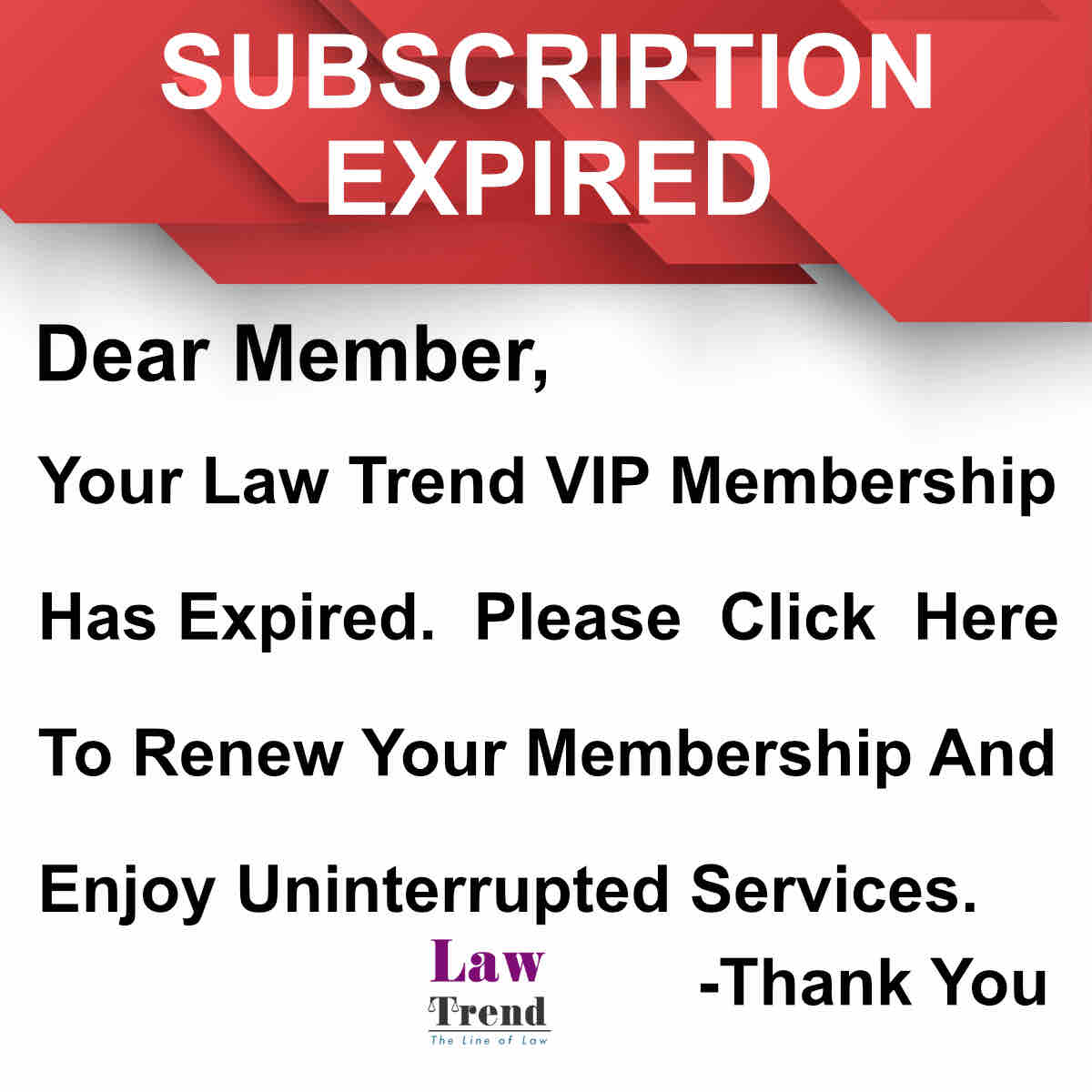कोच्चि इंटरनेशनल फाउंडेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (NUALS) द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने “परिवर्तनकारी संवैधानिकता और न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर प्रभावशाली संबोधन दिया। उन्होंने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की आज भी बनी हुई सच्चाई को उजागर किया, जो संविधान की 75 वर्षों की यात्रा के बावजूद कायम है।
अपने व्याख्यान की शुरुआत श्याम बेनेगल की टेलीविज़न श्रृंखला संविधान के एक दृश्य से करते हुए, जस्टिस मुरलीधर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं के मन में उठ रहे प्रश्नों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “इनमें से कई सवाल आज भी हमारे साथ हैं।” उन्होंने संविधान के समतामूलक दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से साकार करने के संघर्ष को रेखांकित किया।
व्याख्यान का सबसे झकझोर देने वाला क्षण तब आया जब उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की घटना साझा की। उन्होंने कहा, “इलाहाबाद में एक न्यायाधीश ने अपने चैंबर को गंगाजल से शुद्ध किया क्योंकि उसके पूर्ववर्ती दलित थे। ये हमारे समाज की कठोर सच्चाइयाँ हैं।”
जस्टिस मुरलीधर ने ऐसे कई और उदाहरण दिए जहाँ जातीय और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह आज भी गाँवों और शहरों में जीवित हैं। “दलित दूल्हा अपनी ही शादी में घोड़ी नहीं चढ़ सकता,” उन्होंने कहा। “ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दलितों को स्वतंत्र रूप से चलने नहीं दिया जाता। शहरी इलाकों में मुस्लिमों को मकान किराये पर नहीं दिए जाते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें भी बहिष्कृत किया जाता है।”
उन्होंने इन उदाहरणों को संविधान की परिवर्तनकारी दृष्टि—विशेषतः अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23—के लिए एक सीधा खतरा बताया। “अगर इन अनुच्छेदों को गंभीरता से लागू किया जाता, तो आज भी अछूत प्रथा नहीं होती,” उन्होंने कहा। एक और घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “सत्तारूढ़ दल के एक विधायक ने अपने घर को इसलिए शुद्ध किया क्योंकि उसमें पहले एक दलित रहा था। उसे सार्वजनिक रूप से फटकार मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने यह काम बिना किसी संकोच के किया।”
संविधान को ‘उधार की विचारधारा’ कहने वाले आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त प्रावधानों को चुना और उन्हें भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया। उन्होंने जोड़ा, “और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो केवल भारतीय संविधान में ही मिलते हैं।”
उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में निहित “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान हमें अधिकार नहीं देता, बल्कि उन्हें मान्यता देता है। “संविधान की प्रस्तावना वितरणात्मक न्याय और प्रभावी समानता की बात करती है, केवल औपचारिक समानता की नहीं। यह इस उद्घोषणा से शुरू होती है कि हमने स्वयं को यह संविधान दिया है—यह अधिकार किसी और ने नहीं, हमने स्वयं निर्धारित किए हैं।”
डॉ. बी.आर. आंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में सबसे बड़ी अनुपस्थिति समानता और बंधुता की रही है। उन्होंने कहा, “हमारा संविधान आकांक्षात्मक था, लेकिन जब तक हम रोजमर्रा के जीवन में मौजूद अन्याय का सामना नहीं करते, तब तक हम उस आकांक्षा से पीछे रहेंगे।”
यह व्याख्यान न्यायपालिका की भूमिका को केवल संविधान की व्याख्या तक सीमित नहीं, बल्कि उसके परिवर्तनकारी वादे को साकार करने की जिम्मेदारी के रूप में देखने की एक गंभीर याद दिलाता है।